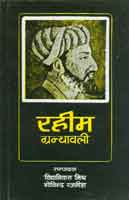|
विविध धर्म गुरु >> रहीम ग्रन्थावली रहीम ग्रन्थावलीविद्या निवास, गोविन्द रजनीश
|
181 पाठक हैं |
||||||
इसमें रहीम द्वारा लिखित रहीम ग्रन्थावली का वर्णन किया गया है...
Rahim granthavali
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
रहीम का संवेदनशील एवं संचेतनशील व्यक्तित्व था। कूटनीति और युद्धोन्माद के विषम परिवेश में उनकी संवेदनशीलता को नष्ट नहीं किया था। इससे उनके अनुभव समृद्ध हुए हैं तथा मानव प्रकृति को समझने का अच्छा अवसर मिला है। वे स्वयं रचनाधर्मी की ओर उन्मुख हुए ही, साथ ही अकबर के दरबार को कवियों और शायरों का केन्द्र बना दिया। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता और उदारवादी नीति ने उन दरारों को पाटने का कार्य किया जो सम्प्रदायों के बीच चौड़ी व गहरी होती जा रही थीं। रहीम जन्म से तुर्क होते हुए भी पूरी तरह भारतीय थे। भक्त कवियों जैसी उत्कट भक्ति चेतना, भारतीयता और भारतीय परिवेश से गहरा लगाव उनके तुर्क होने के एहसास को झुठलाता सा प्रतीत होता है।
प्राक्कथन
‘रहीम-ग्रन्थावली’ रसखान रचनावली के बाद एक विशेष ग्रन्थमाला के क्रम में हाथ में ली गयी। मध्यकाल के बहुत से ऐसे कवि हैं, जिनकी काव्यभूमि बड़ी व्यापक है और जिनकी संवेदना जनमन-स्पर्शिनी है, पर ये कवि लोकप्रिय होते हुए भी काव्यजगत् में अभी उचित रूप में समादृत नहीं हुए हैं, क्योंकि इनकी ऐतिहासिक भूमिका को ठीक तरह समझा नहीं गया है। इन कवियों के प्रमुख ऐतिहासिक भूमिका यह है कि इन्होंने मजहब से ऊपर उठकर मानव भाव को परखा है और दरबारी परिवेश में पले होकर भी जनजीवन में ये पगे हुए हैं। रहीम की रचनाएँ कई बार कई स्थानों से छपीं, जिनका विवरण अन्त में दे दिया गया है, पर अभी तक समग्र संकलन नहीं छपा था, इसलिए पूर्व सामग्री को समाविष्ट करते हुए नूतन सामग्री (जो पांडुलिपियों से प्राप्त हुई। जोड़कर यह संकलन तैयार किया गया है। इसमें विस्तृत भूमिका और शब्दार्थ टिप्पणी जोड़ी गयी हैं।
पूर्व प्रकाशित सामग्री का बहुत बड़ा भाग हमें आगरे के चिरंजीव पुस्तकालय से प्राप्त हुआ, इसके लिए हम श्री देवराज पालीवाल के कृतज्ञ हैं। संकलन डॉ. गोविन्दप्रसाद शर्मा रजनीश ने तैयार किया और विभिन्न स्रोतों से सामग्री लेकर उन्होंने परिश्रम पूर्वक जीवन-चरित भी भूमिका के रूप में प्रस्तुत किया उन्हें मैं साधुवाद देता हूँ। वाणी प्रकाशन ने सुरुचिपूर्वक इसे प्रकाशित किया उनके प्रति आभारी हूँ।
‘रहीम ग्रन्थावली’ हिन्दी के एक बहुत बड़े पाठक समुदाय की आकांक्षा की पूर्ति है, हमें इसके प्रकाशन से बहुत परितृप्ति मिली है। हमें विश्वास है कि यह ग्रन्थावली रहीम के पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रेरणा देगी।
पूर्व प्रकाशित सामग्री का बहुत बड़ा भाग हमें आगरे के चिरंजीव पुस्तकालय से प्राप्त हुआ, इसके लिए हम श्री देवराज पालीवाल के कृतज्ञ हैं। संकलन डॉ. गोविन्दप्रसाद शर्मा रजनीश ने तैयार किया और विभिन्न स्रोतों से सामग्री लेकर उन्होंने परिश्रम पूर्वक जीवन-चरित भी भूमिका के रूप में प्रस्तुत किया उन्हें मैं साधुवाद देता हूँ। वाणी प्रकाशन ने सुरुचिपूर्वक इसे प्रकाशित किया उनके प्रति आभारी हूँ।
‘रहीम ग्रन्थावली’ हिन्दी के एक बहुत बड़े पाठक समुदाय की आकांक्षा की पूर्ति है, हमें इसके प्रकाशन से बहुत परितृप्ति मिली है। हमें विश्वास है कि यह ग्रन्थावली रहीम के पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रेरणा देगी।
विद्यानिवास मिश्र
काव्य यात्रा
भक्तियुग ने विशाल मानवीय बोध जगाया, इसी के कारण रहीम, रसखान जैसे कवि व्यापक भाव बोध के साझीदार हुए। लोगों ने मान लिया है कि भक्ति काल हिन्दू नवजागरण का काल है। भक्ति काल को लोगों ने इस रूप में देखा ही नहीं कि वह सम्पूर्ण मानव के जागरण का काल है, मनुष्य के भीतर सोये हुए बड़े विराट् अनुराग के जागरण का काल है। इसीलिए वह हिन्दू को मुसलमान शासन के प्रतिरोध के भाव से नहीं भरता, वह इतना ही करता है कि हिन्दू और मुसलमान सब को किसी और शासन की प्रजा बनाता है, ऐसे शासन की प्रजा बनाता है जिसमें न हिन्दू रह जाता है न मुसलमान मुसलमान। शासन भी शासन नहीं रह जाता, वह प्रजा की इच्छा से शासित हो जाता है।
भक्तियुग की यह भूमिका थी, कि रहीम और रसखान जैसे शासक वर्ग के लोगों में महाभाव की आकांक्षा जगी, भक्ति से प्रेरित होकर बिना हिन्दू हुए, हुए वैरागी हुए भी आसानी से सुलभ नहीं है। इन कवियों ने भक्ति की वास्तविक भूमिका ठीक तरह से समझी। भक्तिकाल की वास्तविक भूमिका ठीक तरह से समझी। भक्तिकाल की वास्तविक भूमिका है साधारण व्यक्ति की साधारण मनोवृत्ति में असाधारण, अलौकिक की संभावना देखना।
यह भूमिका लाचार करती है कि न केवल साधारण जन की भाषा, उसकी भंगिमा और उसके परिवेश में गहरे रँग जाओ, उसके मन को भी अपनी मन बना लो। रहीम और रसखान ने यही किया। रहीम के अवध क्षेत्र में रहने के कारण अवधी का रंग अधिक गहरा है, हालाँकि उनकी सूक्तियों पर कबीर की भी छाप है, और कृष्ण भक्त कवियों में हरिराम व्यास और सूर की भी छाप है, परन्तु विशेष रूप से तुलसी के साथ उनका तादात्म्य भाषा और भाव दोनों ही दृष्टि से अधिक गहरा है, दोनों ने एक दूसरे से लिया है। कहीं-कहीं तो दोनों के दोहे बिलकुल मिल जाते हैं, जैसे-
भक्तियुग की यह भूमिका थी, कि रहीम और रसखान जैसे शासक वर्ग के लोगों में महाभाव की आकांक्षा जगी, भक्ति से प्रेरित होकर बिना हिन्दू हुए, हुए वैरागी हुए भी आसानी से सुलभ नहीं है। इन कवियों ने भक्ति की वास्तविक भूमिका ठीक तरह से समझी। भक्तिकाल की वास्तविक भूमिका ठीक तरह से समझी। भक्तिकाल की वास्तविक भूमिका है साधारण व्यक्ति की साधारण मनोवृत्ति में असाधारण, अलौकिक की संभावना देखना।
यह भूमिका लाचार करती है कि न केवल साधारण जन की भाषा, उसकी भंगिमा और उसके परिवेश में गहरे रँग जाओ, उसके मन को भी अपनी मन बना लो। रहीम और रसखान ने यही किया। रहीम के अवध क्षेत्र में रहने के कारण अवधी का रंग अधिक गहरा है, हालाँकि उनकी सूक्तियों पर कबीर की भी छाप है, और कृष्ण भक्त कवियों में हरिराम व्यास और सूर की भी छाप है, परन्तु विशेष रूप से तुलसी के साथ उनका तादात्म्य भाषा और भाव दोनों ही दृष्टि से अधिक गहरा है, दोनों ने एक दूसरे से लिया है। कहीं-कहीं तो दोनों के दोहे बिलकुल मिल जाते हैं, जैसे-
पात पात को सींचिबो, बरी बरी को लोन।
तुलसी खोटे चतुरपन, कलि डहके कहु कोन।
तुलसी खोटे चतुरपन, कलि डहके कहु कोन।
-तुलसी
पात-पात को सींचिबो, बरी बरी को लोन।
रहिमन ऐसी बुद्धि को, कहो डरैगो कोन ?
रहिमन ऐसी बुद्धि को, कहो डरैगो कोन ?
-रहीम
एक ओर तुसली की सहज सरलता रहीम में संक्रान्त हुई है, जो जनजीवन के साथ गहरे लगाव से आयी है, दूसरी ओर फारसी और ब्रजभाषा के काव्य की बंकिमा पूरी भावुकता के साथ उनके काव्य में संक्रान्त हुई है, इसके कारण रहीम की काव्य यात्रा अपने समय की साहित्यिक काव्य यात्राओं का संगम बन गयी है। रहीम को सम्पूर्णता में पहचानने का अर्थ होता है, सोलहवीं और सत्रहवीं शताब्दी के साहित्यिक परिदृश्य को पहचानना।
पूरे हिन्दी साहित्य के इतिहास में रहीम एक अद्भुत व्यक्तित्व थे। इतना बड़ा सूरमा कि सोलह वर्ष की उम्र से लेकर बहत्तर वर्ष की उम्र तक निरन्तर कठिन लड़ाइयाँ जीतता रहा। इतना बड़ा दानी कि किसी ने कहा मैंने एक लाख अशर्फियाँ आँख से नहीं देखीं तो एक लाख अशर्फियाँ उसे दे दीं, और उसके साथ ही इतना विनम्र कि किसी कवि ने कहा कि देते समय ज्यों-ज्यों रहीम का हाथ उठता है त्यों-त्यों उनकी नजर नीची होती जाती है और रहीम ने उत्तर दिया :
पूरे हिन्दी साहित्य के इतिहास में रहीम एक अद्भुत व्यक्तित्व थे। इतना बड़ा सूरमा कि सोलह वर्ष की उम्र से लेकर बहत्तर वर्ष की उम्र तक निरन्तर कठिन लड़ाइयाँ जीतता रहा। इतना बड़ा दानी कि किसी ने कहा मैंने एक लाख अशर्फियाँ आँख से नहीं देखीं तो एक लाख अशर्फियाँ उसे दे दीं, और उसके साथ ही इतना विनम्र कि किसी कवि ने कहा कि देते समय ज्यों-ज्यों रहीम का हाथ उठता है त्यों-त्यों उनकी नजर नीची होती जाती है और रहीम ने उत्तर दिया :
देनहार कोई और है भेजते हैं दिन रैन।
लोग भरम हम पर धरैं यातें नीचे चैन।
लोग भरम हम पर धरैं यातें नीचे चैन।
मुझे तो लाज आती है कि लोग भ्रमक्श मुझे देनेवाला समझते हैं, जबकि सचाई यह है कि ‘देनहार’ कोई और है, वही दिन-रात भेजता रहता है। सहृदय ऐसे कि एक सिपाही की स्त्री के इस बरवै पर प्रसन्न हो गये
प्रेम प्रीति को बिरवा चलेहु लगाय।
सींचन की सुधि लीजै मुरझि जाय।
सींचन की सुधि लीजै मुरझि जाय।
और उसे भरपूर धन देकर उसकी नवागत वधू के पास भेज दिया, इसी छन्द में पूरा ग्रन्थ लिख डाला। ऐसे ग्रणग्राही की स्तुति में फारसी और हिन्दी के अनेक कवियों ने स्तुतियाँ लिखीं। जिनमें केशवदास, गंग, मंडन हरनाथ, अलाकुली खाँ, ताराकवि, मुकुन्द कवि, मुल्ला मुहम्मद रजा नवी, मीर मुदर्रिस माहवी हमदानी, यूलकुलि बेग उर्फी, मुल्ला हयाते जीलानी आदि के नाम उल्लेखीय हैं। चरित्रवान ऐसे कि एक रूपवती ने इनसे कहा कि तुम मुझे अपने जैसे पुत्र दो और इन्होंने उसकी गोद में अपना सिर डाल दिया, कहा, एक तो पुत्र हो, न हो, फिर हो तो कैसा हो, इससे अच्छा यही है कि मैं तुम्हारा पुत्र बन जाऊँ।’
भाषाओं के विद्वान ऐसे कि अरबी, फारसी, उर्दू, तुर्की, संस्कृत, इन सब में रचनाएँ कीं और इनमें से प्रत्येक से दूसरी भाषा में हाल के हाल अनुवाद करने में कुशल, प्रसिद्ध ग्रन्थ ‘बाबरनामा’ का तुर्की से फारसी में अनुवाद अपनी युवावस्था में ही इन्होंने पूरा कर दिया था। अभागे ऐसे कि बचपन में बार मरे, मारे मारे फिरे, अकबर ने उन्हें अपने संरक्षण में लिया, अकबर के बड़े विश्वासपात्र बने और अन्त में जहाँगीर और शाहजहाँ दोनों के द्वन्द्व में ऐसे पिसे कि साम्राज्य की सेवा का पुरस्कार यह मिला कि कैद में डाले गये और कैद में ही उनके पास प्रिय पुत्र दाराब खाँ का सिर कटवाकर और एक बर्तन में रखवाकर भेजा गया, यह कहकर भेजा गया कि बादशाह ने तरबूज भेजा है रहीम ने बस आँसू भरे नेत्रों से आसमान की ओर देखा और कहा कि हाँ, यह तरबूज है, अपने जीव-काल में स्वजनों की ही मृत्यु देखी, पहले पत्नी गयी, दो-दो लायक लड़के गये दो-दो लायक दामाद गये तथा पोते भी आँख के सामने मरवा डाले गये। इतने उलट फेर के बाद भी ऐसे स्वाभिमानी कि कभी आन पर आँच आने नहीं दी, चाहे दुःख जितना भी भोगना पड़े।
भाषाओं के विद्वान ऐसे कि अरबी, फारसी, उर्दू, तुर्की, संस्कृत, इन सब में रचनाएँ कीं और इनमें से प्रत्येक से दूसरी भाषा में हाल के हाल अनुवाद करने में कुशल, प्रसिद्ध ग्रन्थ ‘बाबरनामा’ का तुर्की से फारसी में अनुवाद अपनी युवावस्था में ही इन्होंने पूरा कर दिया था। अभागे ऐसे कि बचपन में बार मरे, मारे मारे फिरे, अकबर ने उन्हें अपने संरक्षण में लिया, अकबर के बड़े विश्वासपात्र बने और अन्त में जहाँगीर और शाहजहाँ दोनों के द्वन्द्व में ऐसे पिसे कि साम्राज्य की सेवा का पुरस्कार यह मिला कि कैद में डाले गये और कैद में ही उनके पास प्रिय पुत्र दाराब खाँ का सिर कटवाकर और एक बर्तन में रखवाकर भेजा गया, यह कहकर भेजा गया कि बादशाह ने तरबूज भेजा है रहीम ने बस आँसू भरे नेत्रों से आसमान की ओर देखा और कहा कि हाँ, यह तरबूज है, अपने जीव-काल में स्वजनों की ही मृत्यु देखी, पहले पत्नी गयी, दो-दो लायक लड़के गये दो-दो लायक दामाद गये तथा पोते भी आँख के सामने मरवा डाले गये। इतने उलट फेर के बाद भी ऐसे स्वाभिमानी कि कभी आन पर आँच आने नहीं दी, चाहे दुःख जितना भी भोगना पड़े।
रहिमन मोहि न सुहाय, अमि पियावै मान बिन।
बरु विष देइ बुलाय, मान सहित मरिबो भलो।
बरु विष देइ बुलाय, मान सहित मरिबो भलो।
और ऐसे गहरे प्रेमी कि जिनके भीतर निरन्तर आग लगी रही, पर धुआँ नहीं निकला।
अन्तर दाव लगी रहै, धुआँ न प्रगटै सोय।
कै जिय जानै आपनो या सिर बीती होय।।
यह आग बुझ-बुझ के सुलगती रही :
कै जिय जानै आपनो या सिर बीती होय।।
यह आग बुझ-बुझ के सुलगती रही :
जे सुलगे ते बुझि गए, बुझे ते सुलगे नाहिं।
रहिमन दोहे प्रेम के बुझि के सुलगाहिं।।
रहिमन दोहे प्रेम के बुझि के सुलगाहिं।।
भक्ति की धारा के ऐसे स्नातक कि उन्होंने अपना एक पूरा काव्य ही श्रीकृष्ण को अर्पित किया और जितनी सहजता के साथ उन्होंने श्रीकृष्ण विरह के चित्र खींचे हैं, वह यह कहने को विवश करता है:‘कोटिन हिन्दुन बारिए, मुसलमान हरिजनन पर’। एक ऐसा व्यक्तित्व जो अनुभव का भरा हुआ प्याला हो और छलकने के लिए लालायित हो, मूल के कुल के हिसाब से विदेशी पर हिन्दुस्तान की मिट्टी का ऐसा नमकहलाल कि उसने अपना मस्तिष्क चाहे अरबी, फारसी, तुर्की को दिया हो, पर हृदय ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली और संस्कृत को ही दिया, सारा जीवन राजकाज में बीता और बात उसने की आम आदमी के जीवन की। ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात करते समय बड़ी पीड़ा होती है कि सच्चे अर्थ में हिन्दुस्तानी रंग के इस कवि को कोई समुचित आदर नहीं मिला, रहीम का मजा़र उपेक्षित पड़ा है, वहाँ कोई उर्स नहीं होता, उनके नाम पर कोई अकादमी नहीं है और पठन-पाठन में भी उन्हें स्थान मिलता है तो हद से हद हाई स्कूल तक, ऐसा मान लिया गया है कि वे उपदेशप्रद दोहे-भर लिखते थे। उनकी जिस कविता को उपदेशप्रधान एवं नीतिपरक कहा जाता है, उसकी और जाँच नहीं हुई। जायसी को रामचन्द्र शुल्क मिले पर रहीम को कोई सहृदय समालोचन नहीं मिला।
मैंने जब रहीम के काव्य को पढ़ा तो मुझे लगा कि रहीम का पूरा जीवन चाहे राजसी विलास करते समय, चाहे दर-दर मारे फिरते समय, चाहे फतह करते समय, चाहे कुचालियों के विश्वासघात से शाहंशाह के क्रोध का पात्र होते समय, एक अवाँ था, जो भीतर ही भीतर दहकता रहा।
रहीम के बारे में कहानी मिलती है कि तानसेन ने अकबर के दरबार में पद गाया :
मैंने जब रहीम के काव्य को पढ़ा तो मुझे लगा कि रहीम का पूरा जीवन चाहे राजसी विलास करते समय, चाहे दर-दर मारे फिरते समय, चाहे फतह करते समय, चाहे कुचालियों के विश्वासघात से शाहंशाह के क्रोध का पात्र होते समय, एक अवाँ था, जो भीतर ही भीतर दहकता रहा।
रहीम के बारे में कहानी मिलती है कि तानसेन ने अकबर के दरबार में पद गाया :
जसुदा बार-बार यों भाखै।
है कोऊ ब्रज में हितू हमारो चलत गोपालहिं राखै।।
है कोऊ ब्रज में हितू हमारो चलत गोपालहिं राखै।।
और अकबर ने अपने सभासदों से इसका अर्थ करने को कहा। तानसेन ने कहा कि यशोदा बार-बार अर्थात् पुनःपुनः यह पुकार लगाती है कि है कोई ऐसा हितू जो ब्रज में गोपाल को रोक ले। शेख फैज़ी ने अर्थ किया, ‘बार-बार’ रो-रोकर यह रट लगाती है। खाने आज़म कोका ने कहा, ‘बार’ का अर्थ दिन है और यशोदा प्रतिदिन यही रटती रहती है। अन्त में अकबर ने खानखानाँ रहीम से पूछा। खानखानाँ ने कहा कि तानसेन गायक हैं, इनके एक ही पद को अलापना रहता है, इसलिए इन्होंने ‘बार-बार’ का अर्थ पुनरुक्ति किया। शेख फैज़ी फारसी के शायर हैं, इन्हें रोने के सिवा और क्या काम है। राजा बीरबल द्वार-द्वार घूमनेवाले ब्राह्मण हैं, इसलिए इनको ‘बार-बार’ का अर्थ द्वार ही उचित लगा।
खाने आज़म कोका ज्योतिषी (नजूमी) हैं, उन्हें तिथि वार से ही वास्ता रहता है, इसलिए ‘बार-बार’ का अर्थ उन्होंने दिन- दिन किया, पर हुजूर वास्तविक अर्थ यह है कि यशोदा का बाल-बाल अर्थात् रोम-रोम पुकारता है कि कोई तो मिले जो मेरे गोपाल को ब्रज में रोक ले। इस व्याख्या से न केवल रहीम की विदग्धता और साहित्य की समझ का प्रमाण मिलता है, इससे रहीम के उस गहरे हिन्दुस्तानी रंग का प्रमाण भी मिलता है, जो रोमांच को सात्विक भाव मानता है और रोम- रोम में ब्रह्माण्ड देखता है, जो शरीर के रोम जैसे अंग को भी प्राणों का सन्देशवाहक मानता है, जो वनस्पति मात्र को विराट् अस्तित्व का रोमांस मानता है।
खाने आज़म कोका ज्योतिषी (नजूमी) हैं, उन्हें तिथि वार से ही वास्ता रहता है, इसलिए ‘बार-बार’ का अर्थ उन्होंने दिन- दिन किया, पर हुजूर वास्तविक अर्थ यह है कि यशोदा का बाल-बाल अर्थात् रोम-रोम पुकारता है कि कोई तो मिले जो मेरे गोपाल को ब्रज में रोक ले। इस व्याख्या से न केवल रहीम की विदग्धता और साहित्य की समझ का प्रमाण मिलता है, इससे रहीम के उस गहरे हिन्दुस्तानी रंग का प्रमाण भी मिलता है, जो रोमांच को सात्विक भाव मानता है और रोम- रोम में ब्रह्माण्ड देखता है, जो शरीर के रोम जैसे अंग को भी प्राणों का सन्देशवाहक मानता है, जो वनस्पति मात्र को विराट् अस्तित्व का रोमांस मानता है।
|
|||||
लोगों की राय
No reviews for this book